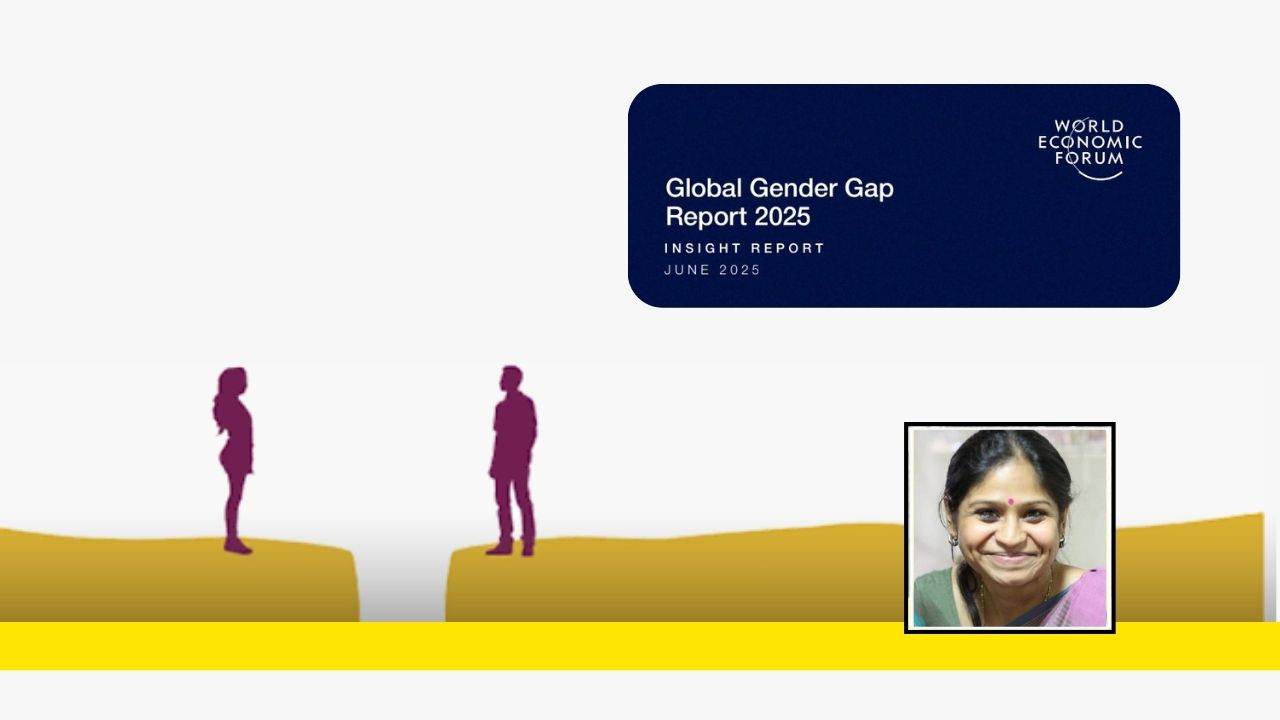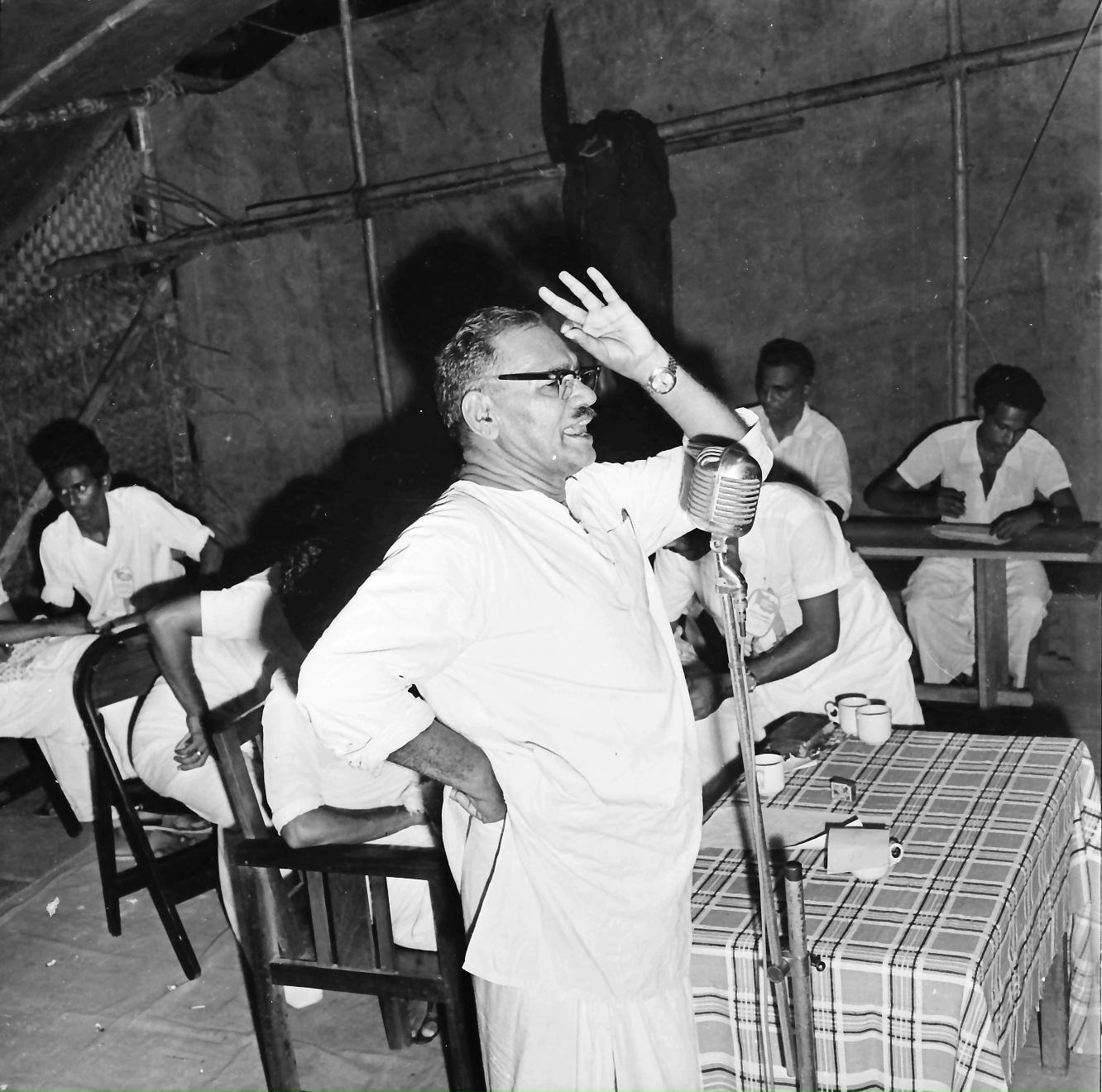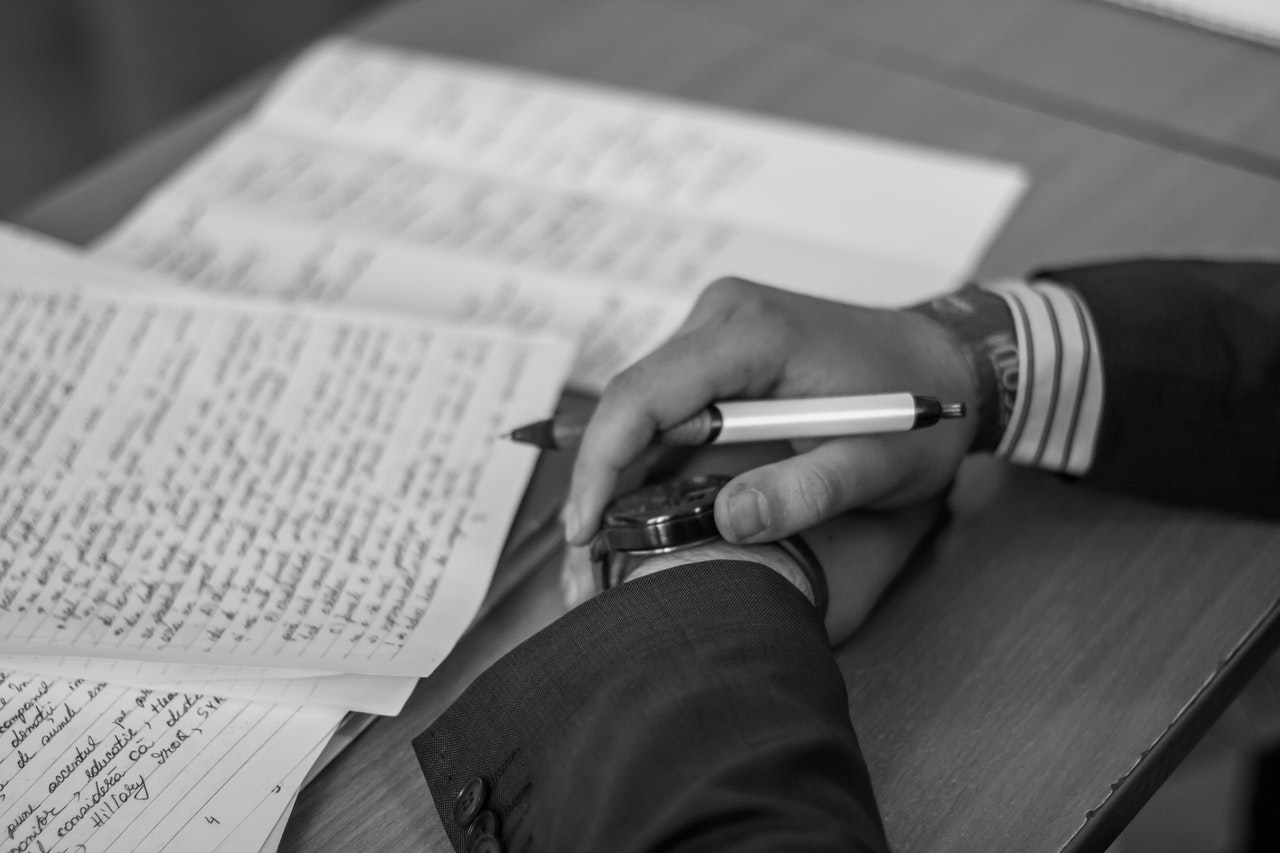सद्भाव के सितार: संगीत और कविता के माध्यम से भारत-ईरानी सांस्कृतिक संबंध

वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नलिन वर्मा का द एआईडीईएम में पाक्षिक कॉलम ‘एवरीथिंग अंडर द सन’ जारी है। यह कॉलम का छठा लेख है।
सभ्यताओं को क्या जोड़ता है? यह समय का बीतना नहीं है, बल्कि उनकी कला की साझा आत्मा है। जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय में, जो कुछ हुआ वह सांस्कृतिक उत्सव से कहीं अधिक था – यह स्मरण का एक अनुष्ठान था, प्राचीन कवियों और उनके संगीत की फुसफुसाहटों द्वारा आकार दिए गए भारत-ईरानी संबंधों की शक्ति का एक जीवंत प्रमाण। यहाँ, कला अभिव्यक्ति एक व्यक्तिगत कार्य नहीं रह गई और एक सामूहिक स्मृति बन गई, जहाँ फ़ारसी छंद और हिंदवी धुनें जड़ों की तरह आपस में जुड़ गईं जो अलग होने से इनकार करती हैं। जैसे-जैसे आधुनिक कलाकारों ने अमीर खुसरो की भावना को आगे बढ़ाया, उन्होंने हमें याद दिलाया कि कोई भी साम्राज्य, कोई भी सीमा, साझा मानवीय कहानियों की प्रतिध्वनि को दबा नहीं सकती। कला न केवल संरक्षित करती है; यह संस्कृतियों के बीच शाश्वत संवादों को जीवित रखते हुए रूपांतरित करती है।
बैंड लीडर और वायलिन वादक मेहरान सेपिडास्ट ने गायक और टार वादक मोर्टेजा फेत्री और अन्य संगीतकारों के साथ मिलकर एक मधुर सिम्फनी बनाई। 7 फरवरी को नई दिल्ली के जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय में यह संगीत दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया।

विश्वविद्यालय और ईरान के दूतावास के सहयोग से आयोजित ईरानी कला दिवस कार्यक्रम के लिए सभागार खचाखच भरा हुआ था। बाहर, दोपहर का सूरज अपनी सुंदर वसंत ऋतु की चमक बिखेर रहा था, लेकिन हॉल की दीवारों के भीतर समय सिमटता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे दर्शक – भारतीय और ईरानी दोनों – हज़ारों वर्षों से चली आ रही भारत और ईरान की साझा सांस्कृतिक विरासत के साथ एक तरह के सम्मोहन में बंध गए।
ये आधुनिक समय के गायक, संगीतकार और कहानीकार थे, फिर भी उनकी कला 13वीं सदी के रहस्यवादी, कवि और संगीतकार अमीर खुसरो की विरासत को प्रतिध्वनित करती थी। फ़ारसी और हिंदवी में उनके छंद और गीत भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य पूर्व में संगीत और साहित्यिक समारोहों के केंद्र में बने हुए हैं।
अतिथियों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय के फिल्म एवं नाटक क्लब की उपाध्यक्ष नुदरत मोइनी ने खुसरो की यह पंक्ति सुनाईः
“ज़े-हाल-ए-मिस्कीन मकुन तग़ाफुल दुरा.ए नैनां बाना.ए बतियाँ
की तब-ए-हिज्रां नादरम ऐ जान न लेहू काहे लगा.ए छतियाँ”
[मेरी दयनीय स्थिति के प्रति उदासीन मत रहो,
तुम्हारी आँखें दूसरी ओर चली जाती हैं, जबकि तुम्हारे शब्द धोखा देते हैं।
क्योंकि मैं इस विरह की पीड़ा को सहन नहीं कर सकता,
हे प्रियतम, तुम मेरे हृदय को इतना क्यों घायल करते हो?]
इस रोमांटिक पंक्ति का पहला भाग फ़ारसी में है, जबकि दूसरा भाग हिंदवी में है। इस तरह के भाषाई सम्मिश्रण के माध्यम से खुसरो ने हिंदवी का बीड़ा उठाया – खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा और बुंदेलखंडी जैसी क्षेत्रीय बोलियों का मिश्रण, जिसमें फारसी भी शामिल थी – जिसने वर्तमान हिंदी क्षेत्र के साहित्यिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया।
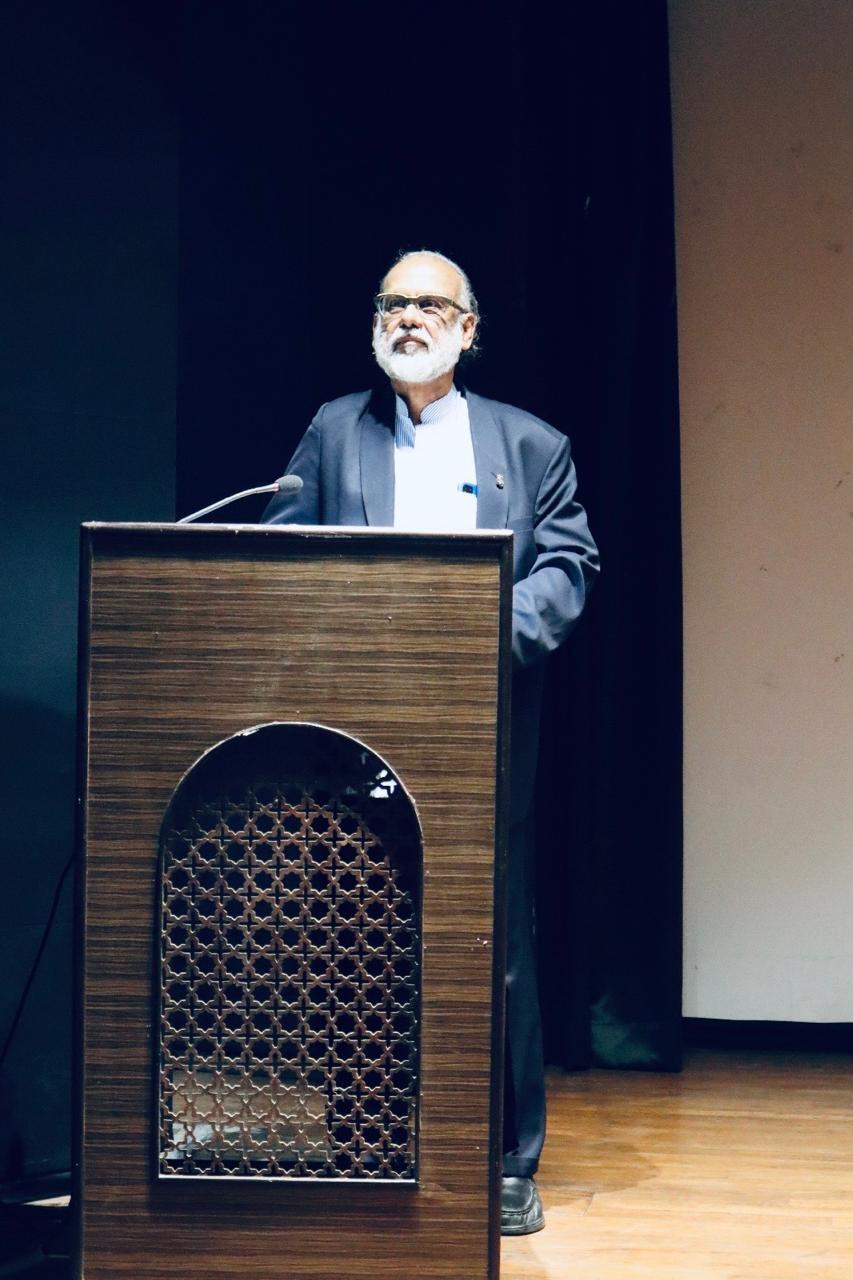
कला, साहित्य, लोकगीत और संगीत में अमीर खुसरो की अद्वितीय प्रतिभा की बराबरी करना मुश्किल है। उन्होंने भारतीय और फ़ारसी संगीत परंपराओं को सहजता से मिलाया, जिससे कव्वाली और ग़ज़ल जैसे नए रूप सामने आए, जो सूफ़ी और भक्ति संतों के पसंदीदा माध्यम बन गए। ये शैलियाँ दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में सांस्कृतिक और साहित्यिक समारोहों में पनपती रहती हैं।
ख़ुसरो जितने कवि थे, उतने ही कुशल संगीतकार भी थे। उन्होंने तीन-तारों वाली त्रितंत्री वीणा को सितार में बदला – जिसे इस कार्यक्रम में मोर्टेज़ा फ़ेत्री ने बजाया – तबला पेश किया, जो अब भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपरिहार्य है, और भारतीय धुनों में कई तुर्क-फ़ारसी तत्वों को शामिल किया। उन्होंने घोरा और सनम जैसे नए राग भी पेश किए, जो ईरानी कला दिवस समारोहों में गूंजे और भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और व्यापक अरब दुनिया में शास्त्रीय और लोक संगीतकारों के बीच पसंदीदा बने रहे।
पारखी:
इस सांस्कृतिक संगम की संकल्पना और मंच तैयार करने का श्रेय जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) मोहम्मद अफशर आलम को जाता है। वे प्रशिक्षण से कंप्यूटर और इंटरनेट वैज्ञानिक हैं, साथ ही वे फारसी और हिंदुस्तानी संगीत और साहित्य के भी पारखी हैं।
प्रो. (डॉ.) रेशमा नसरीन, डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर (DSW) और सेंटर फॉर मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन स्टडीज (CMMS) की निदेशक ने इस आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक सशक्त और क्रियाशील महिला, उन्होंने इस दृष्टि को जीवन में लाने के लिए अथक प्रयास किया।
सांस्कृतिक समन्वयक प्रो. खुर्शीद अहमद अंसारी ने फिल्म एवं नाटक क्लब के अध्यक्ष जावेद अहमद और ‘साज’ म्यूजिक क्लब की अध्यक्ष डॉ. कल्पना जुत्शी के साथ मिलकर इस अवसर को और भी भव्य बना दिया। उन्होंने कलाकारों, लेखकों, दास्तानगोई कथावाचकों और संगीतकारों को उर्दू और हिंदी में समृद्ध भाषणों के माध्यम से सम्मानित किया।
विदेशी छात्र संघ (एफएएस) की प्रमुख प्रो. (डॉ.) जीनत इकबाल ने ईरानी बैंड, कलाकारों और विद्वानों के साथ सहयोग को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि यह कार्यक्रम कलात्मक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक सच्चा उत्सव बन गया।
ईरानी कला दिवस ने आत्मा को भरपूर पोषण देने के अलावा, दर्शकों – ज्यादातर विद्वानों, छात्रों और कला और साहित्य के पारखी – के बीच यादों की बाढ़ ला दी, जिसमें सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य पूर्व के सांस्कृतिक ताने-बाने में गहराई से समाए लोककथाएँ, गाथाएँ, कविताएँ, छंद और गीत शामिल थे।

कई मायनों में, जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय के मनोरम परिसर में आयोजित यह कार्यक्रम भारत और ईरान तथा व्यापक रूप से मध्य पूर्व के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई संबंधों को समृद्ध और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह संस्थान के लिए गर्व का क्षण था, जिसके चांसलर हम्माद अहमद, हकीम हाफिज अब्दुल मजीद के वंशज हैं – एक दूरदर्शी चिकित्सक और परोपकारी व्यक्ति जिन्होंने दक्षिण दिल्ली के हृदय में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में पहचाने जाने वाले संस्थान की नींव रखी।

फ़ारसी लंबे समय से भारत की साहित्यिक विरासत का एक अविभाज्य हिस्सा रही है। मुगल काल की प्रशासनिक भाषा के रूप में अपनी स्थिति से परे, इसने रचनात्मक और संचार क्षेत्रों में व्याप्त होकर साहित्य, लोककथाओं, किंवदंतियों और परंपराओं के धन को जन्म दिया। अगर मिर्ज़ा ग़ालिब और अल्लामा इक़बाल जैसे कवियों ने फ़ारसी और हिंदवी में अपनी कविताएँ लिखीं – जो बाद में उर्दू और हिंदी में विकसित हुईं – तो अनगिनत मनमोहक लोककथाएँ और गाथाएँ भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य पूर्व के बीच यात्रा करती रहीं, जिससे दोनों संस्कृतियाँ समृद्ध हुईं।
रोमांस और लेखक
संगीत और कविताएँ रोमांस को जगाती हैं और अपने दर्शकों को खुशी देती हैं, लेकिन लेखकों का जीवन शायद ही कभी उतना रोमांटिक या आसान होता है जितना कि उनके द्वारा रचित छंद और धुनें। ईरानी उपन्यासकार मुस्तफ़ा मस्तूर ने अपने मुख्य भाषण में इस वास्तविकता को व्यक्त किया:

x“चतुर लोग लेखक नहीं बनते। एक लेखक सड़कों पर पीड़ित लोगों का दर्द महसूस करता है; वह उनके दुख और पीड़ा के साथ जीता है। कोई नाटक या उपन्यास के दुखद तत्वों का आनंद ले सकता है, लेकिन एक लेखक को त्रासदी के शक्तिशाली कार्यों को गढ़ने के लिए उन भावनाओं को सहना चाहिए। चतुर लोग पीड़ितों के दुख में डूबने के लिए अपना आराम नहीं छोड़ते। लेकिन लेखक चतुर लोग नहीं होते… वे ऐसा करते हैं।”
कनाडाई नाटककार, कवि और दास्तानगो कलाकार जावेद दानिश ने अपने एकल नाटक ‘हां, मेरा राजी ऑटिस्टिक है’ को पढ़कर दर्शकों की आंखें नम कर दीं। दुनिया भर की 50 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवादित इस नाटक में एक माँ की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है, जो अपने ऑटिस्टिक बेटे के साथ ज़िंदगी गुज़ारती है।
ईरानी गायकों और संगीतकारों के बैंड, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले कवियों और उपन्यासकारों, तथा हीर-रांझा और सोहनी-महिवाल की चिरस्थायी भावना अमर रहे – वे महान प्रेमी जिनकी कहानियां भारत और मध्य पूर्व के दर्शकों को आकर्षित करती रहती हैं।
Read in: English